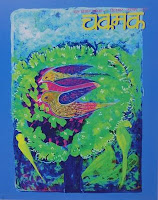Saturday, December 31, 2011
Sunday, December 18, 2011
‘समय से मुठभेड़ ’ करते ‘धरती की सतह पर ’ अदम गोंडवी नहीं रहे
इसे संयोग कहूं या कि दुर्योग कि मेरे ब्लाग पर
क्रमश: यह चौथी पोस्ट है जो किसी के न रहने या न रहे को याद करने की है। पहले हेमराज
भट्ट, फिर पिताजी, संध्या गुप्ता और अब अदम गोंडवी।
Saturday, December 10, 2011
प्रारम्भ में लौटने की इच्छा से भरी संध्या गुप्ता
''मित्रों, एकाएक मेरा विलगाव आप लोगों को नागवार लग रहा है, किन्तु शायद आपको
यह पता नहीं कि मैं पिछले कई महीनों से जीवन के लिए मृत्यु से जूझ रही हूं। अचानक
जीभ में गंभीर संक्रमण हो जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। जीवन का
चिराग जलता रहा तो फिर खिलने-मिलने का क्रम जारी रहेगा। बहरहाल, सबकी खुशियों के
लिए प्रार्थना।''
Saturday, December 3, 2011
घड़ी, लाइन बाक्स, रामपुरी और बाबूजी
 | |
| पीएल पटेल सेवानिवृति बनाम विदाई |
चाबी वाली अलार्म घड़ी बाबूजी ने रेल्वे की नौकरी
में आते ही खरीद ली थी। उनकी नौकरी ही कुछ
ऐसी ही थी। स्टेशन मास्टर होने के नाते उन्हें कभी रात को बारह बजे, तो कभी
सुबह आठ बजे, तो कभी शाम चार बजे डयूटी पर जाना होता था। उनकी डयूटी के ऐसे अटपटे
समय के कारण उनके सोने का समय भी ऐसा अटपटा ही था। 80 से लेकर 1992 में सेवानिवृति तक वे रेल्वे के परिचालन विभाग में उपखंड नियंत्रक से लेकर मुख्य खंड नियंत्रक के पद पर कार्यरत रहे।
Sunday, November 27, 2011
एक अध्यापक की डायरी ....
27 नवम्बर, 2011 को उत्तरकाशी में एक सादे किन्तु गरिमामय समारोह में ' एक अध्यापक की डायरी के कुछ पन्ने' का विमोचन अनंत गंगोला ने किया। इस डायरी में हेमराज भट्ट ने अपने दैनिक अनुभवों को समेटा है। यह डायरी एक अध्यापक के संकल्प एवं व्यवस्था के प्रति पैदा हुए समालोचनात्मक दृष्टिकोण की स्पष्ट छटा दिखाती है। साथ ही एक कर्मठ अध्यापक की जद्दोजहद को भी हमारे सामने रखती है।
यहां प्रस्तुत हैं इस डायरी के तीन पन्ने-
'बालसखा' हेमराज की यादें
 |
| (22.6.1968**25.11.2008) |
मित्रो, पिछले बरस मैंने 25 नवम्बर को यह पोस्ट लगाई थी। 25 नवम्बर,2011 को हेमराज भट्ट की तृतीय पुण्यतिथि थी। यह पोस्ट लगभग ज्यों की ज्यों फिर से प्रस्तुत है। हां इस पोस्ट में जो नई बातें हैं वे इसी रंग में हैं। आपमें से बहुत से साथियों ने इस पर पिछले बरस टिप्पणी की थी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
*
हेमराज भट्ट ‘बालसखा’ से मेरी पहली मुलाकात 2000 के आसपास लखनऊ में नालंदा संस्था द्वारा आयोजित बालसाहित्य निमार्ण की एक कार्यशाला में हुई थी। मैं स्रोत व्यक्ति था और हेमराज भागीदार। कार्यशाला में मैंने उसे एक संकोची, चुप रहने वाले और विनम्र व्यक्ति के रूप में ही जाना था। बाद में सम्पर्क और गहरा हुआ।Tuesday, October 25, 2011
जश्न-ए-बचपन
Wednesday, October 19, 2011
चम्पा और काले अच्छर : त्रिलोचन जी की कविता है
(मित्रो
क्षमा चाहता हूं। 8 सितम्बर को पोस्ट की गई इस कविता के
साथ नागार्जुन जी का नाम चला गया था। त्रिलोचन और नागार्जुन समकालीन कवि हैं। कम से कम मुझे इनमें से जब भी किसी एक की
याद आती है तो बरबस दूसरा भी याद आ ही जाता है। यादों के इस घालमेल में उस समय यह चूक हो गई। आज कर्मनाशा वाले सिद्धेश्वर सिंह जी
ने मेरा ध्यान इस ओर खींचा। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। कविता एक बार फिर से
प्रस्तुत है।)
Sunday, October 16, 2011
शतक ' चकमक ' का
इस 22 अक्टूबर को एकलव्य द्वारा प्रकाशित मासिक बालविज्ञान पत्रिका चकमक के 300 वें अंक का विमोचन
भोपाल के भारत भवन में गुलज़ार कर रहे हैं। चकमक के प्रकाशन का यह 27 वां साल है।
कह सकते हैं एक तरह से चकमक अब परिपक्व हो गई है।
Sunday, September 18, 2011
मुन्ना के मुन्ने दिन
मुन्ना। हां मुन्ना नाम ही था उसका। अरे भई अभी मुन्ना ने स्कूल जाना
कहां शुरू किया था। वह चार साल का ही तो था। मुन्ना के अम्मां-बाबूजी ने जरूर
कुछ सोचा होगा कि जब उसे स्कूल में दाखिल करेंगे तो क्या नाम रखेंगे। अब मुन्ना
को क्या मालूम कि क्या नाम सोचा था उसका ! उससे थोड़े ही पूछा था। बच्चों से
कौन पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम रखें। पूछते तो कितना मजा आता न !
Thursday, September 8, 2011
नागार्जुन: चम्पा और काले अच्छर
कृपया यह पोस्ट देखें।
Friday, September 2, 2011
अपने मियां मिठ्ठू
जाकिर अली 'रजनीश' से उस समय से परिचय है जब यह ब्लाग की दुनिया बनी नहीं थी। वे बालसाहित्य में नए-नए लेखक के रूप में उभर रहे थे। मैं चकमक की सम्पादकीय टीम में था। साहित्य का हिस्सा एक तरह से मेरे ही जिम्मे था। चकमक के 100 अंक पूरे होने वाले थे। जाकिर की कई रचनाएं मैंने सखेद वापस कर दी थीं। एक दिन उनका एक तल्ख पत्र मिला। जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप शायद नामचीन लोगों की रचनाएं ही प्रकाशित करते हैं। जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है उनसे आप बहुत जल्द प्रभावित हो जाते हैं। वास्तव में ऐसा था नहीं। लेकिन इस बात को समझाना बहुत मुश्किल काम था और वह भी एक उभरते हुए लेखक को।
Sunday, August 14, 2011
Sunday, August 7, 2011
Monday, August 1, 2011
गोरख पाण्डेय का गीत समझदारों के नाम
हवा का
रुख कैसा है, हम
समझते हैं
हम उसे पीठ क्यों दे देते हैं , हम समझते हैं
हम समझते हैं खून का मतलब
पैसे की कीमत हम समझते हैं
क्या है पक्ष में विपक्ष में क्या है , हम समझते हैं
हम इतना समझते हैं
कि समझने से डरते हैं और चुप रहते हैं।
हम उसे पीठ क्यों दे देते हैं , हम समझते हैं
हम समझते हैं खून का मतलब
पैसे की कीमत हम समझते हैं
क्या है पक्ष में विपक्ष में क्या है , हम समझते हैं
हम इतना समझते हैं
कि समझने से डरते हैं और चुप रहते हैं।
चुप्पी
का मतलब भी हम समझते हैं
बोलते हैं तो सोच-समझकर बोलते हैं हम
हम बोलने की आजादी का
मतलब समझते हैं
टुटपुंजिया नौकरी के लिए
आजादी बेचने का मतलब हम समझते हैं
मगर हम क्या कर सकते हैं
अगर बेरोजगारी अन्याय से
तेज दर से बढ़ रही है
हम आजादी और बेरोजगारी दोनों के
खतरे समझते हैं
हम खतरों से बाल-बाल बच जाते हैं
हम समझते हैं
हम क्यों बच जाते हैं , यह भी हम समझते हैं।
बोलते हैं तो सोच-समझकर बोलते हैं हम
हम बोलने की आजादी का
मतलब समझते हैं
टुटपुंजिया नौकरी के लिए
आजादी बेचने का मतलब हम समझते हैं
मगर हम क्या कर सकते हैं
अगर बेरोजगारी अन्याय से
तेज दर से बढ़ रही है
हम आजादी और बेरोजगारी दोनों के
खतरे समझते हैं
हम खतरों से बाल-बाल बच जाते हैं
हम समझते हैं
हम क्यों बच जाते हैं , यह भी हम समझते हैं।
हम
ईश्वर से दुखी रहते हैं अगर वह
सिर्फ कल्पना नहीं है
हम सरकार से दुखी रहते हैं
कि समझती क्यों नहीं
हम जनता से दुखी रहते हैं
कि भेड़ियाधसान होती है।
सिर्फ कल्पना नहीं है
हम सरकार से दुखी रहते हैं
कि समझती क्यों नहीं
हम जनता से दुखी रहते हैं
कि भेड़ियाधसान होती है।
हम
सारी दुनिया के दुख से दुखी रहते हैं
हम समझते हैं
मगर हम कितना दुखी रहते हैं यह भी
हम समझते हैं
यहां विरोध ही बाजिब कदम है
हम समझते हैं
हम कदम-कदम पर समझौते करते हैं
हम समझते हैं
हम समझौते के लिये तर्क गढ़ते हैं
हर तर्क गोल-मटोल भाषा में
पेश करते हैं , हम समझते हैं
हम इस गोल-मटोल भाषा का तर्क भी
समझते हैं।
वैसे हम अपने को किसी से कमहम समझते हैं
मगर हम कितना दुखी रहते हैं यह भी
हम समझते हैं
यहां विरोध ही बाजिब कदम है
हम समझते हैं
हम कदम-कदम पर समझौते करते हैं
हम समझते हैं
हम समझौते के लिये तर्क गढ़ते हैं
हर तर्क गोल-मटोल भाषा में
पेश करते हैं , हम समझते हैं
हम इस गोल-मटोल भाषा का तर्क भी
समझते हैं।
नहीं समझते हैं
हर स्याह को सफेद और
सफेद को स्याह कर सकते हैं
हम चाय की प्यालियों में
तूफान खड़ा कर सकते हैं
करने को तो हम क्रांति भी कर सकते हैं
अगर सरकार कमजोर हो
और जनता समझदार
लेकिन हम समझते हैं
कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं
हम क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं
यह भी हम समझते हैं।
0 गोरख पाण्डेय
(1945 में जन्मे और 1989 में इस दुनिया से विदा हुए गोरख पाण्डेय की यह कविता समझदारों के लिए आज भी उतनी ही मौजूं है, जितनी लिखते समय रही होगी।)
Monday, July 18, 2011
काके लागूं पांय....
गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय
बलिहारी गुरु आपकी गोविन्द दियो बताय
 |
| फोटो:राजेश उत्साही |
चरण स्पर्श यानी पैर छूना वास्तव में किसी के प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करने का तरीका है। पर विभिन्न कारणों से यह सत्ता या अपनी प्रभुता
साबित करने का भी एक जरिया बनता रहा है। हमारे समाज में इसके ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। मुझे लगता है इसकी शुरुआत घर से ही होती है।
इसके बारे में पर्याप्त चर्चा किए बिना बच्चों से यह अपेक्षा की जाती रही है कि
वे अपने से बड़ों के पैर छूएंगे, चाहे इसके लिए उनका मन गवारा करे या न करे। दूसरी
तरफ कुछ ऐसे रिश्ते-नाते भी हैं जिनमें पैर छूना अपने आप ही तय मान लिया जाता है। और अगर आप उसका पालन न करें,तो कोपभाजन के लिए तैयार रहें। महिलाओं के साथ तो जैसे यह अनिवार्य शर्त सी हो जाती है। नई-नवेली बहू का ससुराल पक्ष अगर भरा-पूरा हो तो उसकी तो झुक झुककर कमर ही टूट
जाती है।
*
बहरहाल पैर छूने की यह कवायद मेरे लिए बहुत सारी
खट्टी-मीठी यादों का सबब बन गई है। पैर छूने की कोई कट्टरता घर
में नहीं थी। हां जब किशोर हुए तो विभिन्न अवसरों पर यह अपेक्षा होने लगी कि हम
परम्परा का निर्वाह करें। जैसे जन्मदिन और दीवाली आदि पर माता-पिता,दादी और बहनों के पैर छुएं। रक्षाबंधन पर बहनों के। यह आज भी जारी है। कुछ अन्य
मौकों पर अन्य परिचितों के पैर भी छूने की अपेक्षा होती थी। पर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यह बहुत मन से
किया हो। या कि इनमें से किसी भी अवसर पर हम सामने वाले से इतने अभिभूत थे कि बिना
किसी आडम्बर के झुककर सायास ही पैर छू लिए हों। हर बार किसी परम्परा या लिहाज का झंडा आगे-पीछे चलता ही रहा।
*
कुछ ऐसे वाकये या मौके जरूर रहे हैं, जो बरबस याद आ जाते हैं। उत्तर भारत में आमतौर पर सास अपने दामाद के पैर छूती है। लेकिन
मेरे जमीर को यह कभी गवारा नहीं हुआ। जब ऐसा मौका आया, तो मैंने इससे हरसंभव बचने का प्रयास किया। और कई मौकों पर तो उल्टे उनके ही पैर छू लिए। सभी महिलाओं से
चाहे वे रिश्ते में जो भी लगती हों, मैं हमेशा पैर छुवाने से बचता रहा हूं। दक्षिण
भारत स्त्री-पुरुष के बजाय आयु देखी जाती है। यानी
आयु में जो भी छोटा है वह अपने से बड़े के पैर छुएगा ही। यहां बंगलौर में जब मुझे
एक बेटी मिली तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। संस्कारों के चलते मुझे
उसके पैर छूने थे और उसे मेरे। अंत में हम दोनों में समझौता इस बात पर
हुआ कि कोई किसी के पैर नहीं छुएगा।
*
मुझे दो ऐसे वाकये याद आते हैं, जब सचमुच मेरा मन
किया कि सामने वाले के पैर छू लिए जाएं। पहली घटना तीन साल पहले
की है। मेरा पचासवां जन्मदिन था। भोपाल में घर के पास के बाजार में मैं कुछ सामान
खरीदने गया था। वहां अचानक जाने-माने शिक्षाविद् अनिल सद्गोपाल मिल गए। उन्हें
मैं अनिल भाई कहता हूं। 1982 के आसपास उनके साथ काम करने का मौका मिला था। उनकी
कही एक बात मेरे लिए मार्गदर्शक बन गई थी।
होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम की पत्रिका के पहले अंक की सामग्री सीमेंट की खाली बोरी में भरकर उन्होंने मुझे सौंपते हुए कहा था,' कि इसे भोपाल से छपवाकर लाना है।'
मैं अवाक था। कि मैंने ऐसा कोई काम पहले कभी नहीं किया था। हां पढ़ने-लिखने में मेरी रुचि अवश्य रही थी। मैंने कहा था, 'मुझ से यह नहीं होगा। मुझे यह काम नहीं आता है।' उन्होंने तुरंत ही वह बोरा मेरे हाथ से ले लिया और कहा था, 'अगर जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो किसी भी काम के लिए यह मत कहना कि यह मुझे नहीं आता है। कहना कि मैं कोशिश करूंगा। अन्यथा कोई काम करने का मौका नहीं देगा।' फिर तो यह बात मैंने गांठ बांध ली। इस एक सूत्र के सहारे न जाने कितने कौशल मैंने सीखे। काम किए,जिम्मेदारियां उठाईं।
तो पचासवें
जन्मदिन पर आर्शीवाद प्राप्त करने के लिए अनिल भाई से बेहतर कौन हो सकता था।
मैंने झुककर उनके पैर छू लिए। मेरे इस व्यवहार से वे भी हतप्रभ थे। पर जब मैंने
अवसर और अपना मंतव्य उन्हें बताया तो उनकी आंखों में वह चमक उभर आई जो मैं अक्सर देखता था।
*
दूसरी घटना पिछले बरस की है। मैं जयपुर की यात्रा पर
था। रमेश थानवी जी के बारे में पढ़ता और सुनता रहा था। वे राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति में पिछले कई बरसों से सक्रिय हैं। समिति की पत्रिका अनौपचारिका का संपादन कर रहे हैं। वे बच्चों के लिए भी लिखते रहे हैं। उनकी एक मशहूर कहानी 'घडि़यों की हड़ताल' मैंने चकमक में प्रकाशित की थी। लगभग साल भर तक अनौपचारिका के
लिए मैं एक कालम भी लिखता रहा हूं। जयपुर गया तो मैंने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की।
उन्होंने मेरे ठहरने की जगह का पता पूछा और खुद ही कार चलाते हुए मिलने चले आए।
अपने सामने उनको पाकर अनायास ही मैं उनके पैरों में झुक गया। सच कहूं तो उनका व्यक्तित्व
ही ऐसा है।
*
दो और ऐसे व्यक्ति हैं,जिनके मैंने कई अलग अलग मौकों पर बहुत आदर के साथ और मन से चरण स्पर्श किए हैं। इनका मेरे जीवन में स्थान लगभग गुरु जैसा है। एक हैं श्याम बोहरे। श्याम भाई ने मुझे ऐसे समय राह दिखाई, जब मेरे जीवन में लगभग अंधेरा छा गया था। मैं आत्मविश्वास खो चुका था। सच कहूं तो उनकी दिखाई राह पर चलकर ही यहां तक पहुंचा हूं। दूसरे हैं डॉ.सुरेश मिश्र। इन्होंने मुझे कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं उन्हें 'सर' ही कहता हूं। अनजाने में ही मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वे उन व्यक्तियों में से हैं जो लगातार मेरा परिचय मुझ से कराते रहे हैं।
*
दो और ऐसे व्यक्ति हैं,जिनके मैंने कई अलग अलग मौकों पर बहुत आदर के साथ और मन से चरण स्पर्श किए हैं। इनका मेरे जीवन में स्थान लगभग गुरु जैसा है। एक हैं श्याम बोहरे। श्याम भाई ने मुझे ऐसे समय राह दिखाई, जब मेरे जीवन में लगभग अंधेरा छा गया था। मैं आत्मविश्वास खो चुका था। सच कहूं तो उनकी दिखाई राह पर चलकर ही यहां तक पहुंचा हूं। दूसरे हैं डॉ.सुरेश मिश्र। इन्होंने मुझे कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं उन्हें 'सर' ही कहता हूं। अनजाने में ही मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वे उन व्यक्तियों में से हैं जो लगातार मेरा परिचय मुझ से कराते रहे हैं।
*
दो घटनाएं ऐसी भी हैं, जब दो मित्रों को मैंने अपने
पैर छूते हुए पाया। 1990 के आसपास इंदौर का एक युवा जो जनसंचार की पढ़ाई कर रहा
था, छह महीने की इंटर्नशिप के लिए चकमक में आया था। उसे मेरे साथ ही काम करना
था। मेरा काम करने का तरीका कुछ ऐसा था (और शायद अब भी है), मेरी प्रतिक्रिया से लगभग
हर तीसरे-चौथे दिन वह रोने को हो आता। उसकी आंखें भर आतीं। मैं अपनी प्रतिक्रिया को हरसंभव बहुत सहज
तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करता। पर गलत को गलत कहने से बचना मेरे लिए संभव
नहीं था। बहरहाल धीरे-धीरे दिन बीतते रहे। आखिरकार उसके जाने का समय आ गया। चलते
समय औपचारिक अभिवादन के बाद जब सचमुच वह विदा होने लगा तो उसने झुककर मेरे पैर छू
लिए। इस बार आंखें भर आने की मेरी बारी थी। उसने कहा, 'जितना मैंने आपसे इन छह
महीनों में सीखा है, वह शायद छह साल में भी नहीं सीख पाऊंगा।' आज वह इंदौर में जनसंचार पढ़ाता है। हो सकता है वह मुझे भूल गया हो, पर संदीप पारे मैं
तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा।
*
एकलव्य के भोपाल केन्द्र का प्रभारी होने के
साथ-साथ मैं एकलव्य की अकादमिक परिषद का सचिव भी था। इस नाते मेरी दोहरी जिम्मेदारी
थी। एकलव्य में 1997 के आसपास एक नए साथी ने प्रवेश किया। साल भर के बाद जब अकादमिक
परिषद में उनके काम और मानदेय आदि की समीक्षा के बाद पुनर्निधारण हुआ तो वे उससे
संतुष्ट नजर नहीं आए। एक शाम को लगभग दो घंटे इस संबंध में मेरी और उनकी गहन
चर्चा हुई। मैंने संस्था के कार्यकर्त्ता के रूप में, केन्द्र प्रभारी के रूप
में, परिषद के सचिव के रूप में और उससे कहीं आगे बढ़कर एक दोस्त के नाते अपनी बात
उनके सामने रखी। पता नहीं मेरे किस रूप ने यह किया कि चर्चा के बाद वे मुझे एक हद
तक संतुष्ट से लगे। अंतत: जब वे चलने लगे तो उन्होंने झुककर मेरे पैर छू लिए। अनायास
ही किया गया उनका वह अभिवादन आज भी मेरी थाती है। मैं अब एकलव्य में नहीं हूं,
लेकिन राकेश खत्री हैं।
*
सत्ताइस साल का लम्बा अरसा एकलव्य में गुजारने के
बाद अब मैं यहां बंगलौर में हूं। लेकिन जब भी भोपाल जाना होता है, एकलव्य जाता
ही हूं। वहां के दो साथी शिवनारायण गौर और अम्बरीष सोनी जब मिलते हैं तो मेरे पैर
छुए बिना नहीं मानते। पता नहीं उन्होंने मुझमें ऐसा क्या पाया है या मुझसे
क्या पाया है कि वे अचानक ही मुझे जमीन से कुछ ऊपर उठा देते हैं।
0 राजेश उत्साही
Wednesday, July 13, 2011
पच्चीस का कबीर
 |
| नीमा,कबीर और उत्सव |
समय कितनी जल्दी बीत जाता है। जैसे अभी कल ही तो मैंने कबीर पर लिखी एक पोस्ट हमारा कबीर लगाई थी। उसका चौबीसवां जन्मदिन था। आप में से कई साथियों ने अपना आर्शीवाद और शुभकामनाएं उसे दी थीं। देखते ही देखते एक साल बीत गया। आज वह अपना पच्चीसवां जन्मदिन मना रहा है।
एक बार फिर ऐसा मौका है कि मैं यहां बंगलौर में हूं और वह अपनी मां(नीमा) और छोटे भाई उत्सव के साथ भोपाल में। भला हो इस इंटरनेट तकनॉलॉजी का। आज इसके माध्यम से मैंने उसे शुभकामनाओं के साथ लड्डू भेजे और उसने प्राप्त भी कर लिए। बस शायद कुछ बाकी है तो वह आपकी शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो कबीर।0 राजेश उत्साही
Thursday, June 30, 2011
शेष कहानी : वह जो शेष है !
वह दरवाजे के पास ही बैठा था। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। यही कोई 20-22 लोग रहे होंगे। आशा के विपरीत बस अपने निश्चित समय पर रवाना हो गई थी।
हाथ में बैंक काम्पटीशन गाइड जरूर थी पर हिचकोलों के कारण वह ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। वैसे ध्यान भी बराबर वाली सीट पर बैठी दो लड़कियों की ओर था। उम्र में एक-दो साल के अंतर वाली वे लड़कियां बात भी कुछ ऐसी ही कर रहीं थीं, कि किसी को भी सुनने में दिलचस्पी हो सकती थी। छोटी दिखने वाली लड़की बड़ी को मौसी कहकर संबोधित कर रही थी। वह कनखियों से उन्हें देख लेता और फिर गाइड पलटने लगता।
Tuesday, June 28, 2011
कहानी : वह जो शेष है !
वह दरवाजे के पास ही बैठा था। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। यही कोई 20-22 लोग रहे होंगे। आशा के विपरीत बस अपने निश्चित समय पर रवाना हो गई थी।
Wednesday, June 22, 2011
100 वीं पोस्ट .... 26वीं पर 25वीं की याद
पिछली 23 जून को हमारे (नीमा और राजेश) विवाह की पच्चीसवीं वर्षगांठ थी और आज है छब्बीसवीं। तेईस वर्षगांठ हमने होशंगाबाद या भोपाल में ही मनाई थीं। चौबीसवीं वर्षगांठ पर कुछ ऐसा संयोग हुआ था कि हम साथ नहीं थे। और जो हुआ था उस पर मैंने एक पोस्ट ही लिख डाली थी। चाहें तो आप आज भी पढ़ सकते हैं - सालगिरह याद रखने के सत्रह सौ साठ बहाने । लेकिन पच्चीसवीं पर संयोग कुछ ऐसा हुआ कि हम साथ-साथ थे । नीमा मेरे कहने पर अकेले ही भोपाल से 1600 किलोमीटर का लंबा रेल सफर करके बंगलौर आ गई थीं। 23 को हम मैसूर में मित्र सरस्वती के घर थे। उनकी बेटी (जो हमारी भी है) राधा ने एक अनोखा आयोजन हमारे लिए किया। उसने एक-एक गुलाब हमको दिया और आग्रह किया कि हम उसे एक-दूसरे को दें। और कहा कि कसम लें कि अगले पच्चीसों साल तक इसी तरह लड़ते-झगड़ते रहेंगे, पर रहेंगे एक साथ ही। हमने राधा की गवाही में ऐसी ही कुछ कसम ली भी ।
इस साल मैं भोपाल में हूं। सब कुछ वैसा ही है। बस कमी है तो बाबूजी की। वे अब नहीं हैं। बीते बरसों में कई बार हम इस दिन आमने-सामने होते थे। पांव छूते और आर्शीवाद मिलता। और जब नहीं होते तो हम फोन पर पांव छूते और वे फोन की मार्फत ही अपना आर्शीवाद दे देते। आज सुबह होशंगाबाद से मां ने फोन पर वही कहा जो वे हर बरस कहती रहीं हैं-खुश रहो। आवाज नहीं सुनाई दी तो वह केवल बाबूजी की। बहरहाल उनका आर्शीवाद तो साथ है ही। आज ही छोटे भाई अनिल और रानी की शादी की वर्षगांठ भी है।
0 राजेश उत्साही Saturday, June 11, 2011
99....शादी का सातवां फेरा : समापन किस्त
तो लीजिए अपनी भी शादी हो गई। छोटी बहन से लेकर दादी तक सब खुश। सबके तरह तरह के अरमान थे हमारी शादी से जुड़े हुए। शादी के सातवें और अंतिम फेरे यानी सातवीं किस्त में कुछ और यादें।
अगर आपने इसके पहले की छह किस्तें नहीं पढ़ीं हों तो यहां उनकी लिंक है-
Friday, June 3, 2011
98....कोलम्बसी खोज यात्रा का समापन - शादी के लड्डू : 6
2010 की 23 जून को विवाह को पच्चीस बरस हो चुके हैं। इस अवसर पर मैंने गुल्लक पर एक शृंखला शुरू की थी-शादी के लड्डू । इसमें मैं अपने विवाह से जुड़े विभिन्न अनुभवों को आप सबके साथ बांटने की कोशिश कर रहा था। अपरिहार्य कारणों से यह शृंखला अधूरी रह गई थी। 23 जून फिर आ रही है। तो शेष रही कहानी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहें तो इन शृंखलाओं को फिर से पढ़ सकते हैं। लिंक यहां है-
Friday, May 27, 2011
97...एक लुहार की
अगर मैं कहूं कि 9 जुलाई, 2010 का दिन ब्लाग की दुनिया में एक ऐतिहासिक दिन था, तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होनी चाहिए। यही वह दिन था जब डॉ सुभाष राय अपनी बात को कविता में कुछ इस तरह कहते हुए आए-
कबीर ने कहा, आओ
तुम्हें सच की भट्ठी में
पिघला दूं, खरा बना दूं
तुम्हें सच की भट्ठी में
पिघला दूं, खरा बना दूं
Saturday, May 7, 2011
96...व्यथित 'अन्तर्मन '
डॉ. वेद ‘व्यथित’ जी से मेरा पहला परिचय साखी ब्लाग पर हुआ था। वहां उनकी कविताएं प्रकाशित हुईं थीं। आदतन मैंने अपनी टिप्पणी की थी। मुझे याद है मैंने लिखा था ,वेद जी अपनी कविताओं में आत्मालाप करते नजर आते हैं। टिप्पणी थोड़ी तल्ख थी, पर उन्होंने मेरी बात को बहुत सहजता से लिया था। मैं उनका तभी से मुरीद हो गया।
पिछले दिनों मैंने गुल्लक में सुधा भार्गव जी पर एक टिप्पणी लिखी थी और उनकी कविताओं की किताब का जिक्र करते हुए कुछ कविताएं भी दी थीं। संयोग से सुधा जी और वेद जी एक-दूसरे से पहले से परिचित थे, पिछले दिनों दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई तो मेरी चर्चा भी निकल आई। वेद जी ने अपनी हाल ही में प्रकाशित कविताओं का संग्रह अर्न्तमन मुझे कूरियर से भेजा और आग्रह किया कि मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं।
संग्रह के पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा है, ‘सहृदय,सजग साहित्यकार,समर्थ समीक्षक,बेबाक आलोचक व मेरे अभिन्न मित्र राजेश उत्साही को सादर भेंट।’ जब आपको ऐसे विशेषणों से नवाजा जाता है तो आप अचानक ही सजग हो उठते हैं, आपको उन पर खरा उतरने की कोशिश भी करना पड़ती है।
ईमानदारी से कहूं तो वेद जी के संग्रह की कविताएं पढ़ते हुए मैंने यह कोशिश की है। संग्रह में छोटी-बड़ी कुल मिलाकर 80 कविताएं हैं। वेद जी ने संग्रह की भूमिका में लिखा है कि, ‘ये कविताएं स्त्री-विमर्श पर हैं। लेकिन मैंने चलताऊ स्त्री विमर्श के नारे को इनमें कतई नहीं ढोया है। स्त्री विमर्श शब्द आते ही लगने लगता है – शोषित,अबला,सताई हुई,बेचारी दबी कुचली स्त्री या हर तरह से हारी हुई या जिस तरह साहित्यकारों ने उसे इससे भी ज्यादा नीचे दिखाया जाना ही स्त्री विमर्श माना है,परन्तु मेरा ऐसा मानना नहीं है। ऐसा कहना स्त्री के प्रति एक प्रकार का अन्य है।'
ज्यादातर कविताओं में वेद जी अपनी बात पर अडिग नजर आते हैं। पर आत्मालाप वाली बात मुझे यहां भी नजर आती है। वे अपनी अधिकांश कविताओं में स्त्री से बतियाते नजर आते हैं। पर उनका बतियाना इतना सहज है कि उसमें कोई आडम्बर या लिजलिजापन नजर नहीं आता । आइए कुछ उदाहरण देखें-
तो क्या
मैं यह मानूं
कि जो मैंने सुना है
वह ही कहा है तुमने
यदि हां तो
बस उसकी स्वीकृति में
मात्र हां भर दो
(स्वीकृति)
कवि स्त्री के प्रति इतना प्रतिबद्ध है कि वह ना सुनने के लिए भी तैयार है बिना किसी शिकायत के। वह आशावान है-
अस्वीकृति भले हो भी
तो भी मुझे विश्वास है
कि वह अस्वीकृति हो ही नहीं सकती
क्योंकि कठोर नहीं है
तुम्हारा हृदय
(विश्वास)
स्त्री का यह रूप वेद जी को केवल स्त्री में नहीं प्रकृति में भी दिखाई देता है-
मिट्टी के नीचे
कितने भी गहरे
चले जाएं बेशक बीज
तो भी नष्ट नहीं होते हैं वे
धरती मां अपनी गोद में
दुलारती रहती है उन्हें
(प्यार व दुलार)
पुरुष होने के नाते कहीं-कहीं वे अपराध बोध से भर उठते हैं। लेकिन वे इसे स्वीकारने में हिचकिचाते नहीं हैं-
और मैं अपने अहम् को
बचाए रखने के लिए
कभी बना तुम्हारा देवता
कभी स्वामी और
कभी परमेश्वर
(तुम्हारे प्रश्न)
कितने अपराधबोध ने
ग्रस लिया था मुझे
जब तुम्हारी निरीहता को
अपना अधिकार मान लिया था मैंने
(पुरुषत्व)
(पुरुषत्व)
वेद जी स्त्री के जितने आयाम हो सकते हैं उन सबकी बात करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि उनकी दृष्टि कितने सूक्ष्म अवलोकन कर सकती है। ऐसे अवलोकन करने के लिए धीरज तो चाहिए होता है, धीरज ऐसा जो किसी स्त्री के धीरज की तुलना में ठहर सके। ऐसा मन भी चाहिए जो स्त्री के मन की थाह पाने की न केवल हिम्मत रखता हो बल्कि जुर्रत भी कर सके। वेद जी इन कसौटियों पर खरे उतरते हैं । अपनी कविताओं में वे स्त्री की नेहशीलता,स्त्री की हंसी, उसके हृदय, उसकी क्षमाशीलता, उसकी सहनशीलता, उसकी नियति, उसके समर्पण, उसके मौन, उसके विश्वास, उसके संघर्ष, उसकी शक्ति, उसकी तपस्या, उसके धीरज, उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व और अस्तित्व की बात करते हैं।
कविताएं सहज भाषा में हैं, उन्हें पढ़ते हुए अर्थ समझने के लिए शब्दों में उलझना नहीं पड़ता है। बिम्बों का वेद जी ने भरपूर उपयोग किया है, पर वे भी गूढ़ या अमूर्तता की हद तक नहीं हैं। इन कविताओं को पढ़ना सागर की गहराई में उतरने जैसा है। गहराई में जाने पर आपको ढेर सारे मोती नजर आते हैं। इन मोतियों की चमक से आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। आप तय नहीं कर पाते हैं कि कौन-सा मोती उठाएं। क्योंकि सभी एक से बढ़कर एक हैं। इस संग्रह की हर कविता अपने आप में एक मोती है, लेकिन इन्हें एक साथ देखकर इनकी चमक आपस में इतनी गड्ड-मड्ड हो जाती है कि आप किसी एक को भी अपनी स्मृति में नहीं रख पाते। बहरहाल वेद जी ‘अन्तर्मन’ में तो बस ही जाते हैं।
वे कहते हैं-
मुझे सुनने में क्या आपत्ति है
तुम सुनाओ
मुझे देखने में क्या आपत्ति है
तुम दिखाओ
परन्तु जरूरी है
इसे देखने,सुनने और बोलने में
मर्यादा बनी रहे
हम दोनों के बीच
(मर्यादा)
0 राजेश उत्साही
पुनश्च: भाई सतीश सक्सेना ने याद दिलाया कि व्यथित जी का ब्लाग भी है,शुक्रिया। यह रही उसकी लिंक http://sahityasrajakved.blogspot.com
Monday, April 18, 2011
95...खुशी मिली इतनी कि ..
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक ब्लाक है कुरूद। चार महीने पहले की बात है मैं अपनी मोटरसाइकिल सुधरवाने एक गैरेज में गया। काम थोड़ा ज्यादा था, सो वहां रुकना पड़ा। मैंने देखा कि मोटरसाइकिल सुधारने वाला युवक लगभग हर आधे घंटे बाद गुटखा खा रहा था।
मैंने जिज्ञासा वश उससे पूछ लिया, ‘दिन भर में कितने पैकेट खा लेते हो।’
उसने लापरवाही से उत्तर दिया, ‘यही कोई 25-30 तक।’
मैंने सोचा यह युवक दिन भर में कितना कमाता होगा। उसमें से 25-30 रुपए तो इसी में गंवा देता है। अपनी आदत के मुताबिक मैंने उसे गुटखे के नुकसान और बाकी चीजों पर भाषणनुमा कुछ- कुछ कहा।
उसने उतनी ही लापरवाही से कहा, ‘अरे भैया अब तो यह मरने के साथ ही छूटेगा।’
उसने उतनी ही लापरवाही से कहा, ‘अरे भैया अब तो यह मरने के साथ ही छूटेगा।’
इतनी जल्दी मरने की बात। मैं चुप हो गया।
मोटरसाइकिल ठीक हो गई। मैंने पैसे चुकाए और चलने लगा तो उससे कहा, ‘कल से एक पैकेट कम खाने की कोशिश करना।’
उसने मेरी तरफ देखा और बस मुस्करा दिया।
मैं भी भूल गया। हफ्ते भर बाद मेरा उस ओर से निकलना हुआ तो मुझे याद आया कि चलो एक बार पूछकर देखते हैं क्या हाल है। मुझे देखते ही बोला, ‘भैया 20 तक आ गया हूं।’
इस बार मुस्कराने की बारी मेरी थी।
अब तो जैसे नियम ही बन गया। कोई काम नहीं भी होता तो भी मैं जान-बूझकर हर दूसरे-तीसरे दिन उसके गैरेज के आसपास से निकल जाता। हम एक-दूसरे को देखते, हाथ हिलाकर अभिवादन करते। अभी हाल ही में उससे बात हुई। यह जानकर मैं सुखद आश्चर्य से भर उठा कि अब वह हर रोज केवल तीन-चार पैकेट ही खा रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वह दिन भी जल्द ही आएगा जब वह गुटखा खाना ही छोड़ देगा।
मुझे पता है मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। पर इससे मुझे जो खुशी मिली है वह बहुत बड़ी है। 0 गोवर्धन लाल
Subscribe to:
Posts (Atom)